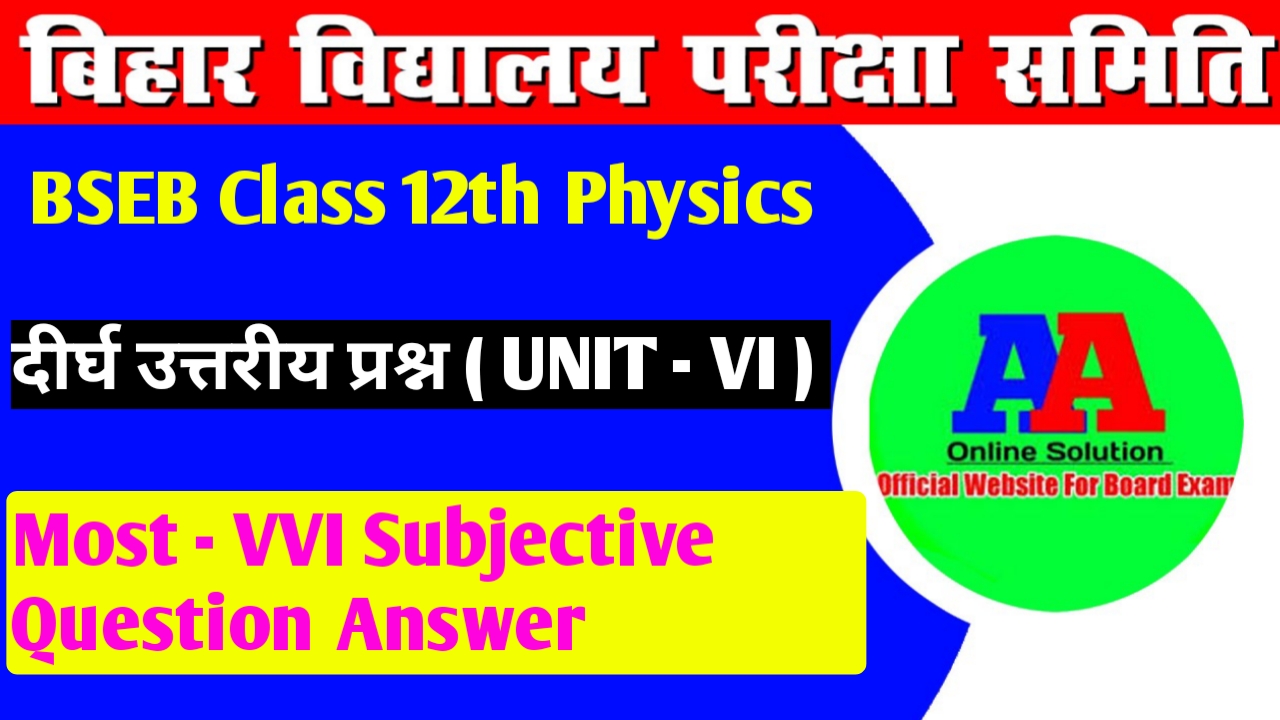BSEB Class 12th Physics Subjective Question 2025 :- दोस्तों यदि आप 12th Exam 2025 Physics Question की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको 12th Physics Question दिया गया है जो आपके 12th Physics Questions And Answers in Hindi PDF के लिए काफी महत्वपूर्ण है | 12th Physics questions and answers | Class 12th Hindi
BSEB Class 12th Physics Subjective Question 2025
1. α-कणों के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन करें एवं निष्कर्ष की विवेचना करें।
उत्तर ⇒ रदरफोर्ड का प्रयोग— रेडियोऐक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित at – कणों के पतले किरणपुंज के सामने धातु की एक पतली पत्ती रखी गई। पत्ती के पीछे जिंक सल्फाइड का पर्दा रखा गया है। धातु की पत्ती द्वारा प्रकीर्णित -कण पर्दे पर स्फुरण पैदा करते थे। स्फुरणों की संख्या गिनकर प्रकीर्णित कणों की संख्या निश्चित की गई।

(i) अधिकांश α – कणों में प्रकीर्णन नहीं होता है
(ii) कुछ α -कण छोटे कणों पर प्रकीर्णित होते हैं।
(iii) अत्यल्प α -कण (10,000 में 1) का प्रकीर्णन 90° से भी अधिक होता है। इस घटना को रदरफोर्ड प्रकीर्णन (Rutherford scattering) कहते है।
व्याख्या (Explanation ) –
परमाणु को ‘न्यूक्लियर मॉडल’ (nuclear model) मानकर रदरफोर्ड प्रकीर्णन’ की व्याख्या की जा सकती है। परमाणु के सभी धनावेश एवं द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर एक अत्यल्प आयतन में सीमित रहते हैं जिसे न्यूक्लियस (nucleus) कहा जाता है। न्यूक्लियस का व्यास करीब 10-14m होता है।
न्यूक्लियस के चारोंओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार वितरित रहते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह वितरित रहते हैं। परमाणु की त्रिज्या करीब 10–10 m होती है। इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर का आकाश लगभग खाली रहता है।
इस प्रकार जब कण का किरणज पतले स्वर्ण-पत्र पर गिरता है तब स्वर्ण-पत्र को बनानेवाली परमाणु के आवेशित न्यूक्लियसों एवं α-कण में टक्कर होता है। चूंकि सोना के न्यूक्लियस की तुलना में α-कण का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए अधिक कोण

पर प्रकीर्णन के साथ-साथ पश्च प्रकीर्णन (back-scattering) की भी व्याख्या हो सकती है। α-कण एवं न्यूक्लियस के बीच कूलॉम का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। α-कण का पथ अतिपरवलय (hyperbola) होता है जिसके बाहरी फोकस (focus) पर न्यूक्लियस रहता है। कणों की प्रारंभिक दिशा एवं अंतिम दिशा के बीच के कोण को प्रकीर्णन कोण (scattering angle) कहते हैं। चित्र में दूरी b को संघात प्राचल (impact parameter) कहते हैं तथा α-कण एवं न्यूक्लियस के बीच की न्यूनतम दूरी को पहुँच की निकटतम दूरी (difference of closest approach) कहते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन-सूत्र (scattering formula) बताता है कि यदि b घटता है तो प्रकीर्णन कोण बढ़ता है। इस प्रकार, जिन -कणों का संघात प्राचल 0 और b के बीच है वे θ से बड़े कोण होकर b प्रकर्णित होगे।

संघाल प्राचल को सीधे मापना संभव नहीं है। ऐसा पाया गया है कि θ कोण पर प्रकीर्णित कणों की संख्या N हो, तो N ∝ cosec4(θ/2) यह संबंध प्रयोग से सत्यापित हो चुका है। N और θ के बीच का संबंध दिखाया गया है।
निष्कर्ष (Inference)- (i) धातु के परमाणु में भीतर धनादेश है जिस कारण परमाणु के समीप से गुजरे कणों पर प्रबल कूलॉम प्रतिकर्षण बल है।
2. बोर के सिद्धान्त के अभिगृहितों को लिखें। बोर के सिद्धान्त पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। अथवा, हाइड्रोजन समान परमाणुओं के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए बोर की मान्यताओं को बताइए तथा किसी परमाणु की स्थायी कक्षा में घूमनेवाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें ।
उत्तर ⇒ बोर के परमाणु मॉडल की आधारभूत अभिधारणाएँ— (i) यह केवल मात्र हाइड्रोजन के समान परमाणु जैसे H, He+ , Li++ आदि के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करता है। यह बहुत से इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए असफल है। (ii) बोर के मॉडल स्पेक्ट्रल रेखा के फाइन संरचना की व्याख्या नहीं करता है।
इलेक्ट्रॉन के लिए कुल ऊर्जा का व्यंजक— माना कि वे कक्षा में इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्रमशः Ek तथा Ep है, तो
Ek = 1/2mV2 ……….(i)

12th Physics questions and answers
3. किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें।
उत्तर ⇒ वह संयंत्र जिससे नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है।

परमाणु रिएक्टर के प्रमुख भाग निम्नलिखित है—
(i) कोर (Core)— यह यूरेनियम की छड़ों का बना होता है जिसपर ऐल्युमिनियम धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है। इसी कोर में ही विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है।
(ii) मंदक या विमंदक— रिएक्टर में ऐसा प्रबंध रहता है कि अवांछित न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाए ताकि नाभिकीय अभिक्रिया अनियंत्रित न हो पाए इसके लिए रिएक्टर के ईंधन में कैडमियम या बोरॉन की छड़े घुसेड़ दी जाती है जो अवांछित न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर उन्हें प्रभावहीन कर देती है। इन छड़ों को मंदक कहते हैं।
(iii) शीतलक—नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे एक द्रव में अवशोषित कर रिएक्टर से हटा लिया जाता है। इस द्रव को शीतक कहते हैं।
(iv) परिरक्षण— यह रिएक्टर का एक प्रमुख भाग है, हालाँकि रिएक्टर के कार्य में यह कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता। इसका कार्य ऊष्मा -किरणों और न्यूट्रॉनों को रिएक्टर से बाहर जाने से रोकना है, ताकि रिएक्टर के निकट काम करनेवाले लोगों को ये कोई नुकसान न पहुँचा सके। यह लगभग 8 फीट मोटे एक विशेष प्रकार के कंक्रीट का बना होता है और यह रिएक्टर को ढँके रहता है।
4. ठोसों के बैंड सिद्धांत को समझाए। इसके आधार पर सुचालक, अचालक तथा अर्धचालक में ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है, लिखें। अथवा, ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है ? इस सिद्धांत के आधार पर [BSEB, 2013] अर्द्धचालक, कुचालक एवं चालक को वर्गीकृत कैसे किया जाता है ?
उत्तर ⇒ ठोसों में ऊर्जा पट्टी — ठोस बहुत सारे एक ही तरह के परमाणुओं से बने
ठोस बहुत सारे एक ही तरह के परमाणुओं से बने
होते हैं। ठोसों में परमाणुओं की अपनी स्थिति स्थिर होती है। जब ठोसों का निर्माण
होता है तो एक परमाणु-दूसरे परमाणु की तरफ गमन करते है। हर वक्त परमाणुओं
के ऊर्जा-स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक एक-दूसरे से क्रिया-प्रतिक्रिया कर
ठोसों की ऊर्जा पट्टी का निर्माण करते हैं।
ऊर्जा बैण्ढ के आधार पर चालकों के लक्षणों की व्याख्या—
चित्रानुसार धातुओं (चालकों) की ऊर्जा बैण्ड रचना वैसी होती है जिसमें कन्डक्शन बैण्ड तथा वैलेन्स बैण्ड एक-दूसरे से ओवरलैप (एक-दूसरे पर चढ़े) होते हैं या कन्डक्शन बैण्ड अंशतः भरे होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भाँति व्यवहार करते हैं। जब चालकों से विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं ।
ऊर्जा बैण्ड के आधार पर अचालकों की व्याख्या—  चित्रानुसारअचालकों में फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल बहुत बड़ा होता है। हीरा के लिए फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल 6eV है, यानी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण भरे बैलेन्स बैण्ड में कन्डक्शन बैण्ड पर कूदने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 6eV लगता है। जब विद्युतीय क्षेत्र फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल वैसे ठोस में आरोपित किये जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को वैसे अधिकपरिमाण के ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है इसलिए कन्ह वैलेन्स बैण्ड जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है अर्थात् वैसे ठोसों से धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये अचालक (कुचालक) कहे जाते हैं।
चित्रानुसारअचालकों में फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल बहुत बड़ा होता है। हीरा के लिए फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल 6eV है, यानी इलेक्ट्रॉन को पूर्ण भरे बैलेन्स बैण्ड में कन्डक्शन बैण्ड पर कूदने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 6eV लगता है। जब विद्युतीय क्षेत्र फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल वैसे ठोस में आरोपित किये जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को वैसे अधिकपरिमाण के ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है इसलिए कन्ह वैलेन्स बैण्ड जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है अर्थात् वैसे ठोसों से धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये अचालक (कुचालक) कहे जाते हैं।
ऊर्जा बैण्ड के आधार पर अर्द्धचालकों के लक्षणों की व्याख्या — चित्रानुसार
चित्रानुसार
अर्द्धचालकों की ऊर्जा बैण्ड संरचना प्रदर्शित है। इसका अन्तराल फोरबीडेन ऊर्जाअचालक की तुलना में बहुत छोटा होता है है। सिलिकॉन के लिए फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल 1.1eV है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक संरचना हीरे की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के समान होती है, किन्तु फोरबीडेन ऊर्जा अन्तराल की कम चौड़ाई के का सरलता से कन्डक्शन बैण्ड में चले जाते हैं, इसलिए सिलिकॉन की चालकता, चालक तथा अचालक के बीच होती है और उसे अर्द्धचालक कहते हैं।
5. रेडियो ऐक्टिव पदार्थ की अर्धआयु एवं औसत आयु से आप क्या समझते है ? रेडियो ऐक्टिव पदार्थ के लिए विघटन सूत्र (N = N0e-λt) स्थापित करें ।
उत्तर ⇒ अर्द्ध-आयु प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है, जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है, उस समय को रेडियो ऐक्टिव का अर्द्ध-आयु कहा जाता है। इसे t1/2 द्वारा सूचित किया जाता है।
∴ t1/2 = 0.693/λ
जहाँ λ = क्षय नियतांक ।
औसत आयु (Average life)— किसी रेडियो ऐक्टिव तत्व के परमाणु की औसत आयु, सभी परमाणुओं के आयुओं के क्षेत्र को परमाणु की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे Ta द्वारा सूचित किया जाता है।
Ta = 1/λ
अतः रेडियोऐक्टिव परमाणु की औसत आयु क्षय नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है।
रेडियोऐक्टिव विघटन का नियम (Law of Radioactive Disintegration)— रेडियोऐक्टिविटी से संबंधित प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि रेडियोऐक्टिविटी विघटन की दर ( rate of disintegration) एक चरघातांकी नियम (exponential law) का अनुसरण करती है तथा यह बताना कि कौन सा परमाणु पहले विघटित होगा, अनिश्चित है; प्रत्येक परमाणु के विघटित होने की संभावना (probability) समान होती है। इस नियम के अनुसार, प्रति सेकेंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यदि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या N है तथा dN परमाणु dt सेकेंड
में विघटित हो जाते हैं, तो विघटन-दर (-dN/dt) कुल परमाणु की संख्या (N) के समानुपाती होती है।
अतः, -dN/dt ∝ N या -dN/dt = -λN …(i)
यहाँ एक नियतांक है जो प्रत्येक रेडियोऐक्टिव तत्त्व के लिए भिन्न होता है। इसे उस रेडियोऐक्टिव तत्त्व का विघटन नियतांक या क्षय नियतांक (disintegration constant or decay constant) कहा जाता है। ऋण-चिह्न से यह प्रकट होता है कि विघटन के फलस्वरूप सक्रिय परमाणुओं की संख्या समय के साथ घट रही है।
समीकरण (i) से,
dN dt = -λdt
समाकलन (integration) करने पर
In N = -λt + c ……..(ii)
जहाँ एक समाकलन नियतांक है। यदि गणना के आरंभ में अणुओं की संख्या N0 हो, अर्थात् t = 0 के लिए N = N0 मान लेने पर
समीकरण (ii) से,
In N0 = -λ × 0 + c = c
अतः समीकरण (ii) में c = In N0 रखने पर,
In N = -λt + In N0 या In N/N0 = -λt
∴ N = N0e-λt
यह नियम रेडियोऐक्टिव विघटन के नियम का गणितीय रूप है ।
12th physics questions for board exam
6. प्रत्यावर्ती धारा उसका महत्तम मान तथा वर्ग-माध्य मूल मान को परिभाषित करें। इनके बीच संबंध स्थापित करें तथा वर्ग माध्य का व्यंजक भी प्राप्त करें । अथवा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान का क्या महत्व है ? इसे परिभाषित करें।
उत्तर ⇒ प्रत्यावर्ती धारा- यदि किसी कुंडली को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समान गति से घुमाया जाता है, तो कुंडली के आधे चक्कर के लिए उसमे प्रेरित वि. वा. बल एक दिशा में तथा शेष आधे चक्कर के लिए वि. व. बल विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त वि. वा. बल का मान प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ऐसी कुंडली के छोरों को किसी परिपथ में जोड़ देने पर परिपथ में भी आधे चक्कर के लिए एक दिशा में और शेष आधे चक्कर के लिए विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। धारा का मान भी प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, इसलिए ऐसा धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं ।
वर्ग-माध्य-मान धारा –
प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग-माध्य मूल धारा का मान पूरे चक्र प्रत्यावर्ती धारा में के औसत वर्गमूल के बराबर होता है। हम जानते हैं कि तात्कालिक प्रत्यावती धारा I = I0 sin ωt तथा इसका आवर्तकाल
T = 2πr/ω ∴ I = I0 sin ωt

Class 12th Board Physics Question
| Class 12th – Physics Objective | ||
| 1 | विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश | Click Here |
| 2 | विद्युत विभव एवं धारिता | Click Here |
| 3 | विद्युत धारा एवं परिपथ | Click Here |
| 4 | विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव | Click Here |
| 5 | चुंबकत्व | Click Here |
| 6 | विद्युत चुंबकीय प्रेरण | Click Here |
| 7 | प्रत्यावर्ती धारा | Click Here |
| 8 | विद्युत चुंबकीय तरंगे | Click Here |
| 9 | किरण प्रकाशिकी | Click Here |
| 10 | तरंग प्रकाशिकी | Click Here |
| 11 | प्रकाश विद्युत प्रभाव | Click Here |
| 12 | परमाणु एवं नाभिक | Click Here |
| 13 | अर्द्ध – चालक युक्तियां : लॉजिक गेट | Click Here |
| 14 | संचार तंत्र | Click Here |